 |
| आचार्य डॉ. मदनगोपाल वाजपेयी |
यह
लेख मैं बहुत दिनों से लिखने पर चिन्तन कर रहा था और अत्यन्त विनम्रता और पीड़ा के
साथ लिख रहा हूँ कि जब आयुर्वेद में ऐसे आचार्यों, टीकाकारों, व्याख्याकारों, लेखकों और फिर चिकित्सकों का प्रवेश हो
जायेगा तो आयुर्वेद की दशा और दिशा क्या होगी? आचार्य चरक, विमान स्थान अ. 8/4 में लिखते हैं कि ‘प्रतिपत्तिज्ञमनुपस्कृतमविद्यमनहङकृतमनसूयकम्।’ अर्थात् आचार्य (अन्य गुणों के
साथ-साथ) अपने कर्तव्य को जानने वाला, अविकृत विद्यायुक्त, अहंकारशून्य तथा गुणों में दोष न देखने
वाला हो, साथ ही वह (शिष्यवत्सलमध्यापकं ज्ञापनसमर्थं चेति।। वि. ८/४।।) आचार्य, अपने शिष्य से इस तरह वात्सल्य (प्रेम)
रखता हो जैसे नवप्रसूता गाय अपने बछड़े से, वह अध्यापन में समर्थ, विषयों के समझाने में चतुर हो। ऐसा
आचार्य अपने सुपात्र/सुयोग्य शिष्यों को ऐसे गुणवान् बना देता है जैसे अच्छे उपजाऊ
जोते हुए खेत को ऋतुकालीन बादल धान्य सम्पन्न कर देते हैं।
जोधपुर (राजस्थान) से आयुर्वेद
विश्वविद्यालय का एक समाचार आ रहा था कि पैसा न देने पर सर्जरी में छात्रों को फेल कर दिया।
यह तो आचार्यों की भयंकर कर्तव्यच्युतता ही
नहीं
बल्कि घोर हैवानियत हो गयी। पर उस स्थिति को आप क्या कहेंगे जहाँ टीकाओं, व्याख्याओं और ग्रन्थों
में
आचार्यों द्वारा भयंकर प्रमाद, कर्तव्यहीनता, विकृतता और दोष छोड़ा गया हो। उसे आचार्य की
ज्ञापन असमर्थता कहेंगे या अज्ञानता इसका निर्णय अब पाठकगण करेंगे।
कुछ माह पहले हमने आयुष ग्राम चित्रकूट में
चिकित्सालय के रोगियों के लिए ‘योगरत्नाकर’ ग्रन्थ के एक औषधकल्प ‘गुल्म कुठार रस’ के निर्माण की तैयारी की। चौखम्बा
कृष्णदास अकादमी से प्रकाशित इस ग्रन्थ के गुल्म रोग प्रकरण में इस रस का वर्णन
है। इसमें पारद न होते हुए भी अपने आशुकारित्व गुण के कारण इसका नाम ‘रस’ रखा गया। ग्रन्थ की निर्माणविधि इस श्लोक में
है-
‘‘नागवङ्गाभ्रकं कान्तं समं ताम्रं समांशकम्।
जम्बीर स्वरसैर्घृष्ट्टवा वटी
गुञ्जाप्रमाणिका।।’’
जिसका अर्थ टीकाकार लिखते हैं कि नाग
भस्म, वंग भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म समभाग, इन सभी को जम्बीरी नींबू के रस के साथ
घोंटकर गुञ्जा (125 मि.ग्रा.) की वटी बनायें। ... ... ... ... ...
... ... ...। यह रस अजीर्ण, आमविकार, गुल्म, हृदय, पार्श्वशूल तथा उदरशूल में प्रयोग करें।
जब हमने मूल श्लोक में दृष्टि डाली तो
देखकर दाँतों के नीचे उँगली दबानी पड़ी कि इतनी अँधाधुन्ध गलती जो दवा और उसकी
केमिस्ट्री ही बदल दे। श्लोक का अर्थ बनता है- (जो संस्कृत
की साधारण सी समझ रखने वाला भी समझ सकता है)।
नाग भस्म, वंग भस्म, अभ्रक भस्म, कांतलौह भस्म। सभी बराबर लेकर इन सभी
के बराबर ताम्र भस्म लेकर यानी नाग, वंग, अभ्रक, कांतलौह 10-10 ग्राम तो ताम्र भस्म 40 ग्राम
लेकर जम्बीरी नींबू के रस में घोंटकर लाल घुंघची (1-1 रत्ती) के बराबर की गोली बना
लें।
अब विचार करें कि योगरत्नाकर की टीका
करने वाले डॉ. इन्द्रदेव त्रिपाठी जो आयुर्वेदाचार्य, बीआईएमएस हैं क्या भाँग खाकर टीका कर
रहे थे?
विचार करें कि यदि इस ग्रन्थ से औषधि
निर्माण करने का इच्छुक व्यक्ति संस्कृत से अनभिज्ञ है तो न तो औषधि निर्माण में
वह कान्तलौह ही डालेगा और न चौगुनी मात्रा में ताम्र। तब तो निर्मित औषधि ही अलग
तरह की बनेगी और काम न करने पर दोष देंगे कि आयुर्वेद काम नहीं करता। ऐसे ही इस
ग्रन्थ की टीका में और भी बहुत सी गल्तियाँ हैं।
बम्बई खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन
बहुत प्रतिष्ठित प्रकाशन माना जाता है। लगभग 115 साल पहले सम्वत् 1963 में यहाँ से
भावप्रकाश (हिन्दी टीका सहित) प्रकाशित हुआ तब से आज तक में इस ग्रन्थ के कई
संस्करण बम्बई से छप चुके। हमारे पास 115 साल पुराना संस्करण भी है और सम्वत् 2076
सन् 2019 का प्रकाशित संस्करण भी है। इस ग्रन्थ के प्राचीन और अर्वाचीन दोनों
संस्करणों में ज्वराधिकार में ज्वर रोगी के लिए एक श्लोक इस प्रकार छपा है-
‘‘ज्वरे प्रमेहो भवति स्वल्पैरपि विचेष्टितै:।
निषण्णं भोजयेन्तस्मान्मूत्रोच्चारौ च
कारयेत्।।’’
भा.प्र.म.ख. ज्वराधिकार २७१।।
जिसका अर्थ लिखा है कि ज्वर में अल्प
चेष्टायें करने उठने-बैठने, चलने-फिरने
से प्रमेह उत्पन्न हो जाता है इस प्रकार ज्वर रोगी जहाँ बैठा हो, वहीं उसे भोजन करा देवें। आदि-आदि।
प्रथम द्ष्ट्या तो भाव प्रकाश में इस
सूत्र को पढ़ने से एक खुशी जैसी मिलती है कि चलो! प्रमेह के अनुसंधान हेतु एकमार्ग
मिला, एक सूत्र मिला। पर जिन्होंनें
शास्त्रों को पढ़ा है, चिंतन
किया है जिन्हें गुरुकृपा प्राप्त है, तंत्रयुक्तियों को पढ़ा है वह तुरन्त ऐसे भँवर
से उबर जाता है, गुरुकृपा से शास्त्र का सही अर्थ स्वत:
स्पष्ट होने लगता है।
दरअसल यह श्लोक भाव प्रकाशकार की रचना
है ही नहीं बल्कि भाव प्रकाश के रचनाकार आचार्य भाव मिश्र ने सुश्रुत संहिता उत्तर
तंत्र ३९/१६२ से इस सूत्र को जैसा का तैसा ही ग्रहण किया है। हमने
पुस्तकालयाध्यक्ष को बुलाकर आयुष ग्राम (ट्रस्ट) के केन्द्रीय पुस्तकालय से
सुश्रुत संहिता के कई संस्करण निकाले और देखा तो पाया कि- सुश्रुत की रचना में इस
श्लोक में ज्वरे प्रमोहो भवति। लिखा है किन्तु भावप्रकाश के मुद्रक ने प्रमोहो कर
प्रमेहो कर दिया। अब कहाँ प्रमेह (Blennorrhagia) और कहाँ प्रमोह (Fainting)। और तो और, सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि
सम्वत् १९९८ में भिषग्रत्न श्री ब्रह्मशंकर मिश्र ने भावप्रकाश की
विद्योतिनी टीका कर चौखम्बा संस्कृत भवन वाराणसी से प्रकाशित कराई उस (भावप्रकाश)
में यही श्लोक 211 क्रमांक पर प्रकाशित है पर उसमें भी प्रमोहो की जगह ‘प्रमेहो’ ही दिया यानी मच्छिका स्थाने मच्छिका। कैसी
विडम्बना
है!
ऐसे ही इसी ग्रन्थ (भावप्रकाश) में
(खेमराज श्री कृष्णदास मुम्बई से) प्रकाशित एक और प्रमाद की चर्चा न करूँ तो
जानकारी अधूरी रहेगी। इस ग्रन्थ में ‘स्वायंभुवगुग्गुलु’ का वर्णन है जो कुष्ठ रोग की अद्भुत औषधि है।
पर जब निर्माण के लिये इसकी हिन्दी टीका देखेंगे तो अन्य घटक द्रव्यों के साथ
नागरमोथा 2 तोला लेने के लिये लिखा है इसके आगे मोथा भी 2 तोला लेने को लिखा है
जबकि सामान्य आयुर्वेदज्ञ तक जानते हैं कि नागरमोथा, मोथा एक ही है और मूल श्लोक में भी ‘मुस्ता’ का एक ही बार उल्लेख है। अब चिन्तनीय बिन्दु तो
यह है कि भावप्रकाश के अनुसार जो कोई स्वायम्भुव गुग्गुलु का निर्माण करेगा तो वह
नागरमोथा दो बार ग्रहण करेगा।
समीक्षा चलते के जब हमने भिषग्रत्न
श्री ब्रह्मशंकर मिश्र द्वारा टीकाकृत और चौखम्बा संस्कृत भवन से प्रकाशित
भावप्रकाश में स्वायम्भुव गुग्गुलु की निर्माण विधि की हिन्दी टीका देखि
तो पाया कि निम्बवह्निसंपाका: का अनुवाद ही नहीं किया गया परिणामत:
घटक द्रव्यों से निम्ब, चित्रक
और अमलतास हट गये। इसी ग्रन्थ में टीकाकार का एक और छोटा सा प्रमाद है किन्तु
महत्वपूर्ण, कृतान्न वर्ग में जब हम तक्र को देखते
हैं तो ग्रन्थकर्ता लिखते हैं कि तक्रं रुचिकरं वह्निदीपनं तृप्तिकारम्।। भा.प्र. पू. ख. कृतान्न की 5/147।।
जिसका सीधा-सीधा अर्थ है कि तक्र, रुचिकर, अग्निदीपक और तृप्तिकारक है। पर मुम्बई
खेमराज प्रकाशक के भावप्रकाश के टीकाकार अर्थ लिखते हैं कि तक्र रुचिकारी, अग्नि का दीपन करने वाला, अत्यन्त पाचक, पेट के सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करने
वाला और तृप्तिकारक है।
मेरी पुत्रवधू डॉ. अर्चना वाजपेयी को
भी मेरी तरह पुस्तकों से बड़ा लगाव है। अभी वे एक लेखक की नवप्रकाशित कायचिकित्सा
के चारों भाग खरीदकर लायीं। मुझे दिखाया, पुस्तक पर मैं विहंगमदृष्टि डालने लगा। इस
पुस्तक में विद्वान् लेखक लिखते हैं कि आयुर्वेद में मानसिक तथा शारीरिक रोगी की
चिकित्सा विधियों को तीन प्रधान वर्गों में विभक्त किया गया है। १- देवव्यापाश्रय
चिकित्सा २- युक्तिव्यापाश्रय चिकित्सा ३- सत्वावजय।
आगे वे लिखते हैं कि ‘‘देवव्यापाश्रय चिकित्सा यह अत्यन्त
प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसका उपयोग मानस रोगों की चिकित्सा तथा रोकथाम के
लिये किया जा सकता है।’’
कितने दु:ख की बात है ये विद्वान् लेखक
जो एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कायचिकित्सा के प्रोफेसर हैं वे छात्रों को देवव्यापाश्रय
चिकित्सा की सीमा मानस रोगों तक बता रहे हैं। जबकि आचार्य चरक ने 11/54 में तीन प्रकार
की औषध बताते हुए सबसे पहले देवव्यापाश्रय चिकित्सा का उल्लेख करके
उसकी
उत्कृष्टता, विराटता सिद्ध की है। विमानस्थान रोगभिषग्जातीय विमानाध्याय 8/87 में
व्यापाश्रय भेद से दो प्रकार की चिकित्सा बतायी हैं तो उनमें भी देवव्यापाश्रय
चिकित्सा को ‘प्रथम’ पर रखा है। देवव्यापाश्रय चिकित्सा में-
‘मंत्रौषधिमणिमङ्गलबल्युपहारहोमनियमयमप्रायाश्चित्तोपवास-स्वस्त्ययनप्रणिपातगमनादि।।’- च.सू. 11/54।। मंत्र जप, औषध एवं मणियों का धारण, मंगलाचार, देवताओं को उपहार, हवन, नियम (भीतर बाहर से पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर उपासना आदि। प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्त्ययन, माता-पिता, गुरु, पूज्यजनों को प्रणाम, तीर्थयात्रा या पवित्र/पुण्यस्थलों की
यात्रा शामिल है। यदि इस कायचिकित्सा के लेखक महोदय चरक संहिता के पहले अध्याय के
ही प्रारम्भिक सूत्र वायु:पित्तं कफश्चोक्त: शारीरो दोषसंग्रह:। मानस:
पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एवं च।।1/57।। और प्रशाम्यत्यौषधै: पूर्वो दैवयुक्तिव्यपाश्रयै:।मानसो
ज्ञानविज्ञानधैर्यस्मृतिसमाधिभि:।।च.सू. 1/58।। पर ध्यान देते तो शायद इतनी भयंकर
भूल नहीं होती। सूत्र 1/57 कहता है कि संक्षेप में वात, पित्त और कफ ये शारीरिक दोष कहे जाते
हैं और फिर रज एवं तम मानस दोष कहे जाते हैं। सूत्र 1/58 स्पष्ट
कहता है कि पूर्व: ·
शारीररोग:
दैवव्यापाश्रय: · देवव्यापाश्रययुक्तिव्यापाश्रयैश्च औषधै: · चिकित्साभि: प्रशाम्यति · शमनं भवति।। यानी शारीरिक रोगों में पहले देवव्यापाश्रय
साथ-साथ युक्तिव्यापाश्रय(औषध, आहार, विहार, पंचकर्म आदि) का प्रयोग करना चाहिए, वे इसी से मिटते हैं।
‘मानस रोगों’ की चिकित्सा में तो महर्षि चरक ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि को कहते हैं (च.सू. 1/58) तथा
उन सभी उपायों को अपनाने की बात बताते हैं जिनसे ‘पुनरहितेभ्योऽर्थेभ्यो मानोनिग्रह:।। च.सू. 11/54।। अहितकर विषयों से मन
नियंत्रित हो सके।
यदि कोई
इन
लेखक महोदय की काय चिकित्सा की पुस्तक में लिखित इस तथ्य को किसी तरह स्वीकार भी कर
ले कि
देवव्यापाश्रय चिकित्सा का उपयोग मानस रोगों की चिकित्सा में ही
है
तो फिर ज्वर चिकित्सा में चरक संहिता चिकित्सा स्थान (3/307-314) में ज्वर मुक्ति
में किये गये उपदेश कि माता-पिता- गुरु सेवा, ईश्वर आराधना, हवन, विष्णुसहस्र नाम पाठ, सज्जन, पुरुषों के दर्शन, वेद श्रवण से मानव ज्वर मुक्त हो जाता
है, की
बात खण्डित हो जायेगी। राजयक्ष्मा चिकित्सा में च.चि. 8/89 में यज्ञ करने का विधान
जैसे देवव्यापाश्रय कर्म का खण्डन हो जायेगा ऐसे ही कुष्ठ रोग के वाग्भट भी
अ.हृ.सू. 1/26 में स्पष्ट बताते हैं- ‘धीधैर्यात्मादि विज्ञानं मनोदोषौषधं परम्।।’ अ. हृ.चि. 19/98 में कुष्ठ जैसे
शारीरिक रोग के उन्मूलानार्थ बतायी देवव्यापाश्रय चिकित्सा कि व्रत, दम, यम, सेवा, त्याग, शील, संस्कारवान् ब्राह्मण, दिव्यात्मा, गुरुपूजा, सभी प्राणियों से मैत्री, शिव परिवार, भगवान सूर्य की आराधना से कुष्ठ रोग
मिटता है इस आर्ष वाक्य का क्या होगा। आचार्य सुश्रुत ने व्रणितोपासना (care of the wounded) अध्याय में व्रणी व्यक्ति के लिए जो कथा, वेद श्रवण, हवन, बलि आदि देवव्यापाश्रय विधान (सु.सू.19/24)
किया है, वह व्यर्थ नहीं हो जायेगा। चरक विमान 3
में जनपदोध्वंस के वर्णन में देवव्यापाश्रय चिकित्सा (3/15-18)पर जो दिया गया है
और तो और यदि चरक विमान 8/9-13 का हम सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो पायेंगे कि
महर्षि चरक ने आयुर्वेद के छात्र/शिष्य के लिए देवव्यापाश्रय अनिवार्य कर्म बताया
है अपने शब्दों में चरक ने यहाँ तक अभिव्यक्ति की है कि बिना देवव्यापाश्रय कर्म
के कोई व्यक्ति आयुर्वेद ज्ञान क्षेत्र में सफल हो ही नहीं सकता।
उधर काय चिकित्सा पुस्तक के विद्वान्
लेखक देवव्यापाश्रय कर्म को मानसिक चिकित्सा की सीमा में बाँधना चाह रहे हैं। इस
समीक्षा को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि अब समय आ गया है कि भारतीय चिकित्सा
राष्ट्रीय आयोग को भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में पूर्व प्रकाशित आर्ष ग्रन्थों की
टीकाओं, नवीन रचनाओं, प्रकाशित पुस्तकों की समीक्षा हेतु एक
समिति या ‘संकाय’ का गठन करना
चाहिए
ताकि पूर्व प्रकाशित आर्ष ग्रन्थों की टीकाओं की समीक्षा और सुधार हो सके तथा
अपरिपक्व लेखकों के लेखन/प्रकाशन तथा टीकाओं पर रोक लग सके तभी आयुष सच्चे विकास
और सुधार में महत्वपूर्ण कार्य होगा, अन्यथा ऐसी रचनायें, टीकायें, नवमनीषी छात्रों, जिज्ञासुओं का भटकाव बनाये रखेगी।
- डॉ. मदनगोपाल वाजपेयी!
इनके शिष्यों, छात्र, छात्राओं की लम्बी सूची है । आपकी चिकित्सा व्यवस्था को देश के आयुष चिकित्सक अनुसरण करते हैं ।
(सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेद हॉस्पिटल)

प्रधान सम्पादक चिकित्सा पल्लव और आयुष ग्राम मासिक
पूर्व उपा. भारतीय चिकित्सा परिषद
उत्तर प्रदेश शासन









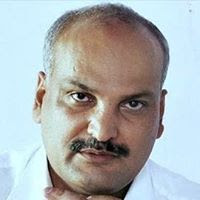







0 टिप्पणियाँ